फ़ुरसत में ... 111
इशक़ वाले लव की तलाश
मनोज कुमार
‘दाग अच्छे हैं’ स्लोगन वाले दौर में कोयला अभी तक काला ही है! किसी ने एक चिंगारी जलाई और ऐसी आग लगी कि ‘शोले’ दहक उठे हैं। ‘शोले’ का फ़ेमस डायलोग तो आपको याद होगा ही, “अब तेरा क्या होगा कालिया?” आज का यह “कालिया” सिर्फ़ ‘सरदार’ का नमक खाने वाला वफ़ादार ही नहीं रह गया है, बल्कि ‘असरदार’ चरित्र-निर्माण, संस्कृति सेवा आदि करने वाले प्रतीकों के रूप में दिख रहा है। अब जब कोयले की आंच से शोले दहके हैं, तो दोनों पक्ष कह ही सकते हैं – “अब तेरा क्या होगा कालिया?”
कोयले का धुंआ प्रदूषण बढ़ाता है। इससे धुंध घनी हो जाती है। धुंध भरी सुबह को तेज़ क़दमों से चलते वक़्त किसी से टकरा जाना अच्छा लगता है। यह अच्छा लगना तब और भी खूबसूरत हो जाता है, जब टकराने वाला आपकी कार्बन कॉपी लगे। इस तरह के व्यक्तित्व से टकराने से जो तड़ित-सम प्रकाश फूटता है, उससे आस-पास छाए धुंध की गहनता विरलता में परिणत होती प्रतीत होने लगती है। मॉर्निन्ग वाक तो एक बहाना होता है, अपन को तो आज भी ट्रैक सूट पहने जॉगिंग कम, चहलक़दमी ज़्यादा करते हुए कुछ ख़ास शक्लों की तलाश रहती है, जो मेरे साहित्य सृजन की प्रेरणा बन सकें। पिछले दिनों इन चेहरों का ऐसा अकाल पड़ा था कि मेरी सृजन-सरिता सूख ही गई थी। आज जब अपने कार्बन कॉपी से टकराया तो बलबला कर सोता-सा फूट पड़ा।
मेरे दिल में सृजन के हज़ारों विषय उथल-पुथल मचाए रहते हैं और दिमाग़ मुझे बराबर ‘यस’ – ‘नो’ के द्वन्द्व में घेरे रहता है – जीवन प्रांगण में आज एक बार फिर से क्रांति की रणभेरी बजने लगी है। मेरी लेखनी का चक्का जाम करने वाले मज़दूर दिमाग के सामने सृजन की क्रांति का मशाल लिए दिल ने मैदान-ए-जंग में डटकर मुक़ाबला किया और अंततोगत्वा जीत मेरी ‘फ़ुरसत’ की ही हुई। विजय के उल्लास में दिल बल्लियों उछल रहा है।
जिससे टकराया था, उसने ‘फ़ुरसत में ..’ मुझे कहीं कुछ पढ़ लिया होगा, और शायद वह मेरी विलक्षण शैली, विनोदी स्वभाव और किस्सागोई का मुरीद भी बन गया हो। लेकिन जिस अंदाज़ में उसने मुझे महिमा-मंडित किया वह उसके मेधावी होने का प्रमाण दे रहा था। हम दोनों उस सैर-सपाटा पार्क के चक्कर लगाते रहे और एक-दूसरे को सुनते-सुनाते रहे। जब मैं अपने विनोदी स्वभाव के नमूने स्वरूप कोई लतीफ़ा सुनाता तो वह पूरी तन्मयता से सुनता और बड़ी ज़ोर से हंसता। फिर वह नहले पर दहला मारने के अंदाज में अपनी बातें रखता और इतने ज़ोर से मेरी पीठ पर धौल जमाते हुए कहता, “बोल गुरु कैसी रही?”
मेरा कार्बन कॉपी मुझे बातों ही बातों में उस जगह ले गया जहां मैं जाना नहीं चाहता था। कहने लगा, ‘यार ! बता – इस जीवन में तूने इकतरफ़ा प्यार कितनी बार किया है?’ मैं चौंका। आश्चर्य और प्रश्न मिश्रित भाव लिए जब मैंने उसके चेहरे की तरफ़ देखा, तो कुछ ज़्यादा ही खुलते हुए उसने कहा, “अरे यार! ‘इशक़’ वाला ‘लव’ … अब भी नहीं समझा? … तूने तो किया, पर उसे पता भी नहीं चला!”
कार्बन कॉपी की बातों से मुझे मेरी ही लिखी हुई एक पंक्ति का स्मरण हो आया – ‘हमारे स्वभाव में ही था झट से किसी के प्रेमपाश में बंध जाना और नसीब में था फट से उस बंधन का टूट जाना।’ ये उन भूले-बिसरे दिनों की नादानियां हैं, जिसे आज मेरे कार्बन कॉपी ने याद दिला दी। पढ़ाई-लिखाई के बीच ‘इशक़’ तो होता था, ‘लव’ नहीं हो पाता था। ‘इशक़’ और ‘लव’ के बीच कैरियर का सांप कुंडली मारकर बैठ जाता और ‘कैरियर चौपट न हो जाए’ की फुंफकार में ‘लव’ की फुसफुसाहट गुम हो जाती थी। ‘स्टुडेंट ऑफ द इयर’ जीत जाता था, लेकिन ‘लवर ऑफ द डे’ भी हार जाता था। हम तो मध्यमवर्गीय बच्चे थे, - जो पालथी मारकर पढ़ते थे। इसलिए हम पढ़ाकू तो बने रहे, - लड़ाकू न बन सके।
आज कार्बन कॉपी ने मेरी इस नादानी को सुन कर मुझे ‘डरपोक’ करार दिया। सच ही तो कहा उसने। मैं क्रांतिकारी तो बन ही नहीं सका। मैंने न कभी क्लास बंक की, न कभी लाइब्रेरी या कैंटिन में बैठा, न कभी नुक्कड़ों पे गॉसिप की, न कभी नौटंकी, सिनेमा, क़व्वाली देखने के लिए रात-रात भर घर से बाहर रहा, न कभी देखी गई फ़िल्म के क़िस्से सुनाने के लिए पार्क में महफ़िल जमाई। कितनी ही चीज़ें छूट गईं या छोड़ता चला गया। शुभचिंतक टाइप के मित्र लानत भेजते। कहते – बड़का प्राइज जीत लेगा। छात्रों में कई उद्दंड किस्म के भी थे, जो पढ़ाकू छात्रों के विकेट उखाड़ने की ताक में लगे रहते थे। उनके बाउंसरों को झेलते हुए ‘पिच’ पर अपनी विकेट सही-सलामत रखना भी बड़े धैर्य और कौशल का काम था। विकेट पर टिके रहना तो आया पर तेज़ी से रन बनाने की कुशलता न आ पाई। लिहाजा छोर बदलने का सिलसिला थमा-सा ही रहा।
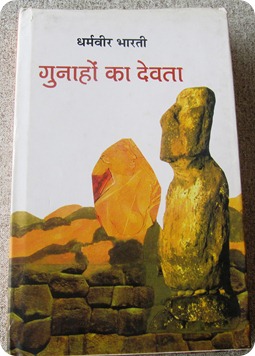 इस तरह से एक उदासीनता द्वारा सर्जित वातावरण में अपनी भावना दबा देने का जो अपराधबोध रहा, उससे मुक्ति के लिए क़लम का सहारा लिया, और गाहे-ब-गाहे फ़ुरसत में कुछ लिख-लिखा लिया। लेकिन उस पढ़ाकू पारिवारिक माहौल में जाने क्यों लिखना भी अपराध माना जाता था। फिर भी, चोरी-छिपे ही सही, लिखने का क्रम ज़ारी रहा। उन दिनों के बड़े-बड़े, नामी-गिरामी, प्रेरक लेखकों की रचनाओं के गहन अध्ययन से दिल से यह आवाज़ उठी कि सतत लेखन के लिए प्रेरक-शक्ति चाहिए।
इस तरह से एक उदासीनता द्वारा सर्जित वातावरण में अपनी भावना दबा देने का जो अपराधबोध रहा, उससे मुक्ति के लिए क़लम का सहारा लिया, और गाहे-ब-गाहे फ़ुरसत में कुछ लिख-लिखा लिया। लेकिन उस पढ़ाकू पारिवारिक माहौल में जाने क्यों लिखना भी अपराध माना जाता था। फिर भी, चोरी-छिपे ही सही, लिखने का क्रम ज़ारी रहा। उन दिनों के बड़े-बड़े, नामी-गिरामी, प्रेरक लेखकों की रचनाओं के गहन अध्ययन से दिल से यह आवाज़ उठी कि सतत लेखन के लिए प्रेरक-शक्ति चाहिए। – अब यह शक्ति या प्रेरणा तो किसी के ‘इशक़’ में पड़ कर ही प्राप्त की जा सकती है। समस्या यह कि मुझ जैसे निठल्ले के लिए ऐसी प्रेरणा उपलब्ध होना एक टेढ़ी खीर थी। एक तरफ़ जहां लड़कियां मां-बाप, समाज से डरती थीं, वहीं दूसरी तरफ़ हमारे ‘लव गुरु’ ऐसे थे जिन्होंने अपनी किताब लिख कर कहा था, “इस उपन्यास का लिखना मेरे लिए वैसा ही रहा है जैसा पीड़ा के क्षणों में पूरी आस्था से प्रार्थना करना; और इस समय भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वह प्रार्थना मन ही मन दोहरा रहा हूं।” जी हां, उन दिनों “गुनाहों का देवता” मध्यमवर्गीय जीवन की कहानी ही तो थी। आदर्श प्रेमिका की जो छवि उसमें गढ़ी गई थी उसे आज तक खोज रहा हूं। मिली नहीं। मुश्किल हमारी यह थी कि बिना इस प्रेरणा के लिख कैसे पाऊंगा? इसलिए झूठ-सच का झट से वाला ‘इशक़’ और फट से वाला ‘ब्रेकअप’ गढ़ता गया और रचता गया।
जो गुनाह कभी किया नहीं, उस गुनाह को बार-बार दुहराता रहा। लेकिन मेरा कार्बन कॉपी उसे मानने के लिए कत्तई तैयार नहीं है। किसी ने कहा है, ‘इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है, जितना कोशिश करने वालों से छूट जाता है।’ पता नहीं मैंने इंतज़ार नहीं किया या कोशिश नहीं की। लेकिन तलाश मेरी बदस्तूर ज़ारी है। इंशा अल्लाह, अगर कभी यह तलाश पूरी हुई तो ‘फ़ुरसत में...’ ज़रूर मिलेंगे। और अगर इस तलाश में आप मेरी मदद कर सकें, तो ज़रूर ख़बर कीजिएगा। त्त-उम्र एहसानमन्द रहूँगा!






 मनोज कुमार
मनोज कुमार  अरुण चन्द्र रॉय की ताज़ी कविता
अरुण चन्द्र रॉय की ताज़ी कविता 



