राष्ट्रीय आन्दोलन
277. संगीत और वैष्णव जन भजन
तिरंगा झंडा का
अपनाया जाना
झंडे का सवाल सबसे पहले 1917 में कांग्रेस के कलकत्ते अधिवेशन में पेश हुआ।
होमरूल लीग ने पहले ही एक तिरंगे झंडे को अपना रखा था। कलकत्ते अधिवेशन में एक
कमेटी नियुक्त की गई जो झंडे का नमूना निश्चित करे। प्रसिद्ध कलाकार अवनिन्द्र नाथ
ठाकुर भी इस कमेटी में थे। लेकिन इस कमेटी की कभी बैठक ही नहीं हुई। इसलिए नागपुर कांग्रेस में गांधीजी के आग्रह पर होमरूल का तिरंगा
झंडा कांग्रेस के झंडे के रूप में अपनाया गया। 1921 में इसमें चरखा जोड़ दिया गया। जब झंडे पर विचार करने के लिए एक
कमेटी बनी तो उसके सुझाव पर लाल रंग की जगह केसरिया अपना लिया गया। यह झंडा आज़ादी
की लड़ाई का गौरवशाली प्रतीक बन गया। इसके सफेद भाग के बीच में नीले रंग का चरखा
था। केसरिया रंग जो ऊपर में था, बलिदान का प्रतीक था। सफेद रंग सादगी और शांति का
और हरा रंग शस्य श्यामला भूमि का। चरखा हमारी अर्थव्यवस्था और स्वावलंबन का प्रतीक
था। स्वतंत्रता के बाद भारत का झंडा भी यही रहा। चरखे की जगह इसमें अशोक चक्र आ
गया।
राष्ट्रीय गीत का अपनाया जाना
आरंभ में कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश साम्राज्य का राष्ट्रीय गीत ‘गॉड सेव द
किंग’ गाया जाता था। 1920 में उसका औचित्य समाप्त हो गया
था। जब ब्रिटिश साम्राज्य ही स्वीकार नहीं था, तो सत्याग्रहियों को उसके राष्ट्रीय
गीत से क्या लेना-देना? इस अधिवेशन से बंकिम चंद्र का ‘वंदे मातरम्’ हर अधिवेशन
में गाया जाने लगा।
संगीत और
वैष्णव जन को
गांधीजी का मानना
था कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक उसमें संगीत न
हो। संगीत को वो सत्याग्रह से लोगों को जोड़ने का एक तरीका उसे मानते थे। वो 15वीं
शताब्दी के सन्त नरसी मेहता का ‘वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाणे रे।’ (सच्चा वैष्णव वही
है, जो दूसरों की
पीड़ा को समझता हो।) गाते थे। महात्मा
गांधी के नित्य की प्रार्थना में यह भजन भी सम्मिलित था। यह उनका बहुत प्रिय भजन था। वे 'रघुपति राघव राजा
राम' भी बहुत तन्मयता से गाते थे। 'वैष्णवजन' को बाद में मिश्र
खमाज़ में लोगों ने ढाला और एमएस सुब्बुलक्ष्मी और पंडित जसराज ने उसकी धुन बनाई
और उसको गाया। दूसरे गानों में भी उनकी दिलचस्पी थी। जब वो यरवदा जेल में थे और
दलितों के पक्ष में आंदोलन करने जा रहे थे, आमरण अनशन पर
बैठने जा रहे थे तो अनशन पर बैठने से पहले उन्होंने सरदार पटेल को और महादेव देसाई
को बुलाया और एक गीत गाने लगे। और वो गीत था, 'उठ जाग मुसाफिर
भोर भई अब रैन कहां जो सोवत है ' और उसके बाद सरदार
पटेल और महादेव देसाई सबने गाना शुरू किया। फिर जेल में जितने और कैदी थे उन्होंने
भी गाना शुरू कर दिया और एक पूरा माहौल बन गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए
गांधीजी लंदन में थे और ठहरे थे मुरिएल लेस्टर के यहां। गांधीजी रोज शाम को जब भी
फारिग होते बाकी काम करने से, बैठकें करने से तो
किंग्सले हॉल के सभागार में चले जाते थे। वहां कुछ स्थानीय लोग इकट्ठा होकर एक
गाना गाते थे। एक स्कॉटिश गीत। स्कॉटलैंड का एक लोकगीत था जिसको रॉबर्ट बर्न्स ने
बाद में नए ढंग से लिखा। आउड लैंग साइन यानी गए ज़माने की बात। गांधीजी वो गीत सुनने के लिए कितनी बार गए, लोगों को अंदाज़ा
नहीं हुआ और फिर गांधीजी को पता चला कि हर शनिवार को लोग इस गाने पर नाचते हैं। उन्होंने
मना करने की कोशिश की। गांधीजी नहीं माने और एक दिन शनिवार को जब वो वहां पहुंचे
और गाना शुरू हुआ और अचानक एक महिला ने हाथ उठाकर कहा कि गाना रोक दो। फिर उसने
गांधीजी की तरफ देखकर कहा कि आप हमारे साथ नाचना चाहेंगे? गांधीजी ने देखा
कि वहां जितने लोग थे वो या तो पति पत्नी थे या दोस्त थे लेकिन एक लड़का, एक लड़की साथ में
नाच रहे थे। गांधीजी ने कहा जरूर, मैं नाचूंगा लेकिन एक शर्त पर कि मेरा जोड़ीदार
मेरी छड़ी होगी और गांधीजी अपनी छड़ी के साथ किंग्सले हॉल के उस सभागार में नाचे।
*** *** ***
मनोज कुमार
पिछली कड़ियां- राष्ट्रीय आन्दोलन
संदर्भ : यहाँ पर
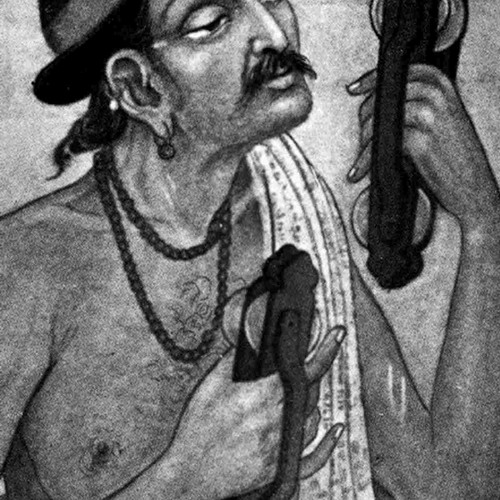
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
आपका मूल्यांकन – हमारा पथ-प्रदर्शक होंगा।